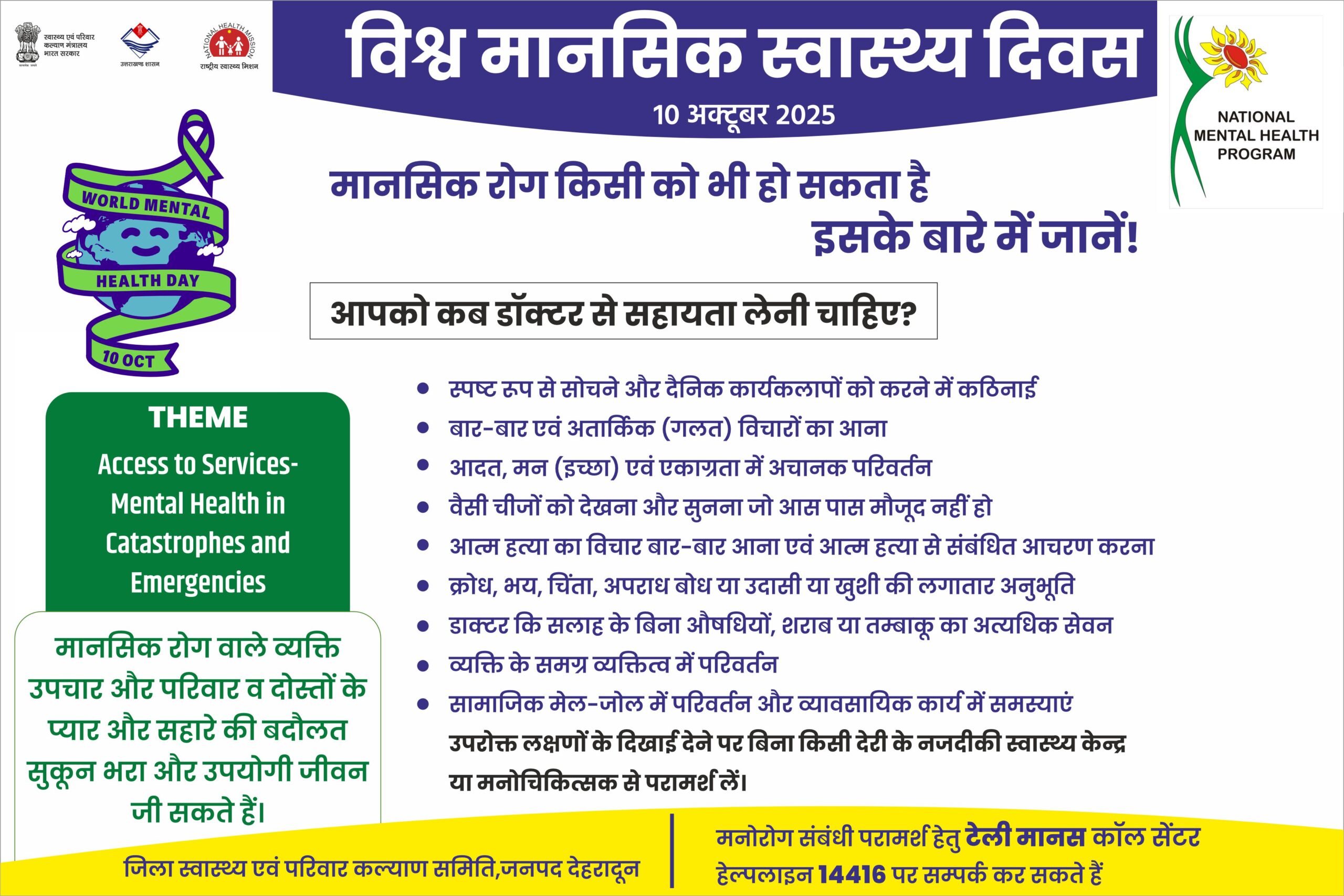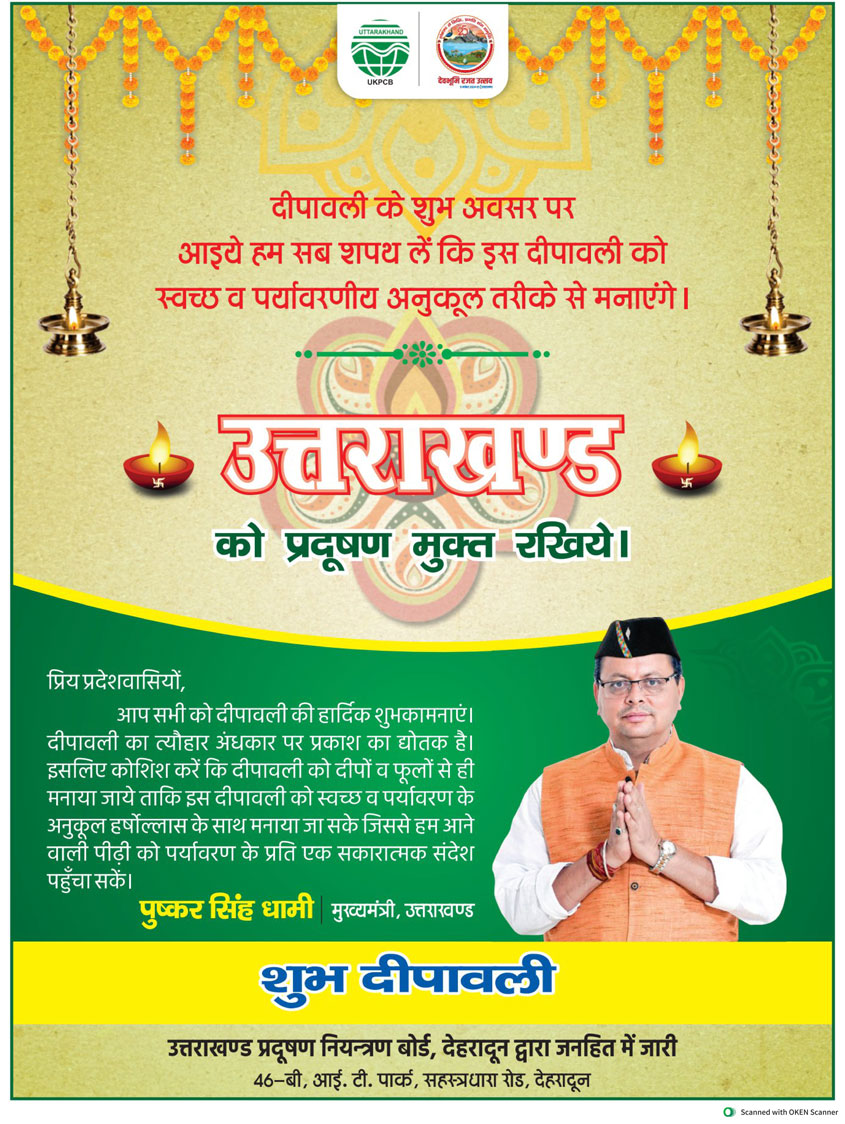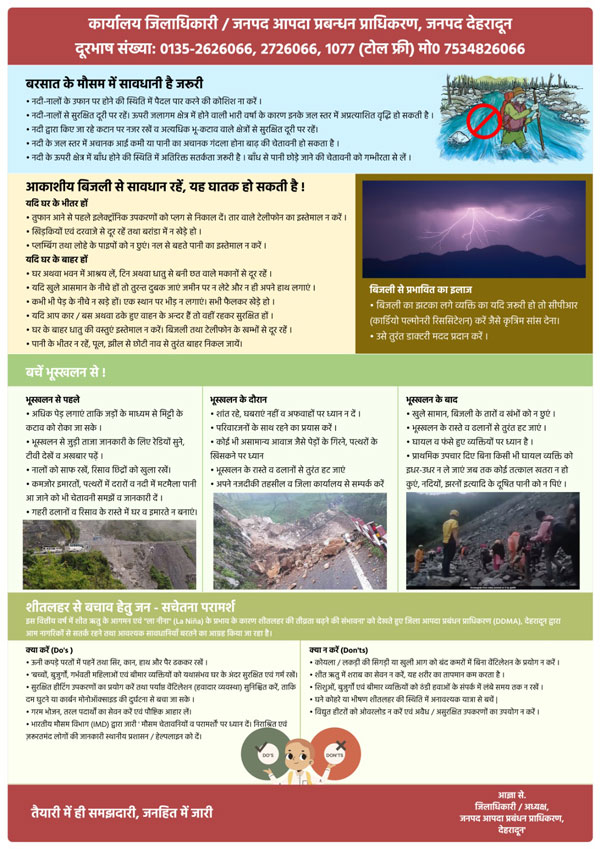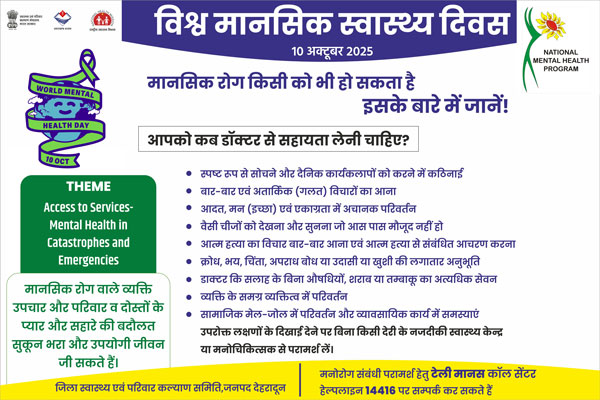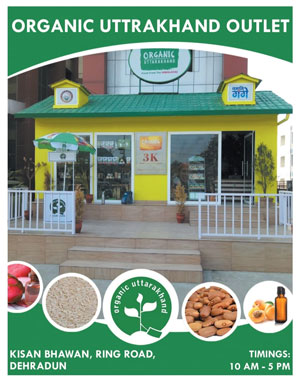नई दिल्ली। संभवत: शिक्षा और रोजगार में आरक्षण भारत के गैर-भेदभाव और समानता कानून में सबसे पेचीदा मुद्दों में से एक है। इसको लेकर असहमति की रेखाएं तब और गहरी हो गईं जब इस हफ्ते की शुरुआत में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में सीटें आरक्षित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के आरक्षण के भीतर सब-कैटेगरी को वैध ठहराया गया। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने सुनाया पांच से अधिक जजों वाली ऐसी पीठ तब गठित की जाती है, जब मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इस मामले में संवैधानिक चिंताएं क्या थीं।
देविंदर सिंह केस
देविंदर सिंह मामले में विवाद 1975 में शुरू हुआ था, जब पंजाब सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर अनुसूचित जातियों (शिक्षा और रोजगार में) के लिए मौजूदा 25 प्रतिशत आरक्षण को दो कैटेगरी में विभाजित कर दिया था, जबकि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित इन सीटों में से आधी सीटें बाल्मीकि और सिखों को दी जानी थीं, बाकी सीटें अनुसूचित जातियों की कैटेगरी के तहत आने वाले अन्य समूहों के लिए आरक्षित थीं.यह अधिसूचना 2004 तक स्थगित रही, जब तक कि ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य केस में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आ गया। इसमें कहा गया कि एससी और एसटी सूचियां एक समरूप समूह को दर्शाती हैं, और एससी/एसटी सूची के भीतर किसी भी अन्य वर्गीकरण या समूहीकरण के खिलाफ फैसला सुनाया. एससी के खास संदर्भ में, संविधान का अनुच्छेद 341, खंड (1) भारत के राष्ट्रपति को यह अधिसूचित करने की शक्ति देता है कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में कौन सी जातियां, नस्लें या जनजातियां (या उनमें समूह) एससी मानी जाएंगी।
पंजाब सरकार ने बनाया कानून
ईवी चिन्नैया मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के भीतर कोई भी सब-कैटेगरी अनुच्छेद 341(1) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ होगी, जो संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है. ईवी चिन्नैया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर 1975 की अधिसूचना को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया था. इन न्यायिक निर्णयों को पार करने के लिए, पंजाब सरकार ने पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 नामक एक कानून बनाया.अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए इस कानून में धारा 4(5) के तहत यह प्रावधान किया गया था कि सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे की 50फीसदी रिक्तियां, अगर उपलब्ध हों, तो अनुसूचित जातियों में से पहली वरीयता के रूप में बाल्मीकि और सिखों को दी जाएंगी। इस विशिष्ट प्रावधान – धारा 4(5) – को 2010 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया था।पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई। मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा गया, जिसे अन्य बातों के अलावा यह तय करना था कि ईवी चिन्नैया मामले में 2005 के फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए या नहीं. 2020 में सुनवाई शुरू हुई, लेकिन चूंकि संविधान पीठ समान संख्या वाली पीठ द्वारा दिए गए पिछले फैसले को पलट नहीं सकती, इसलिए मामले को उच्च पीठ को भेज दिया गया मामले को 2023 में सात न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया, जिसकी सुनवाई अंतत फरवरी 2024 में हुई।
6-1 के बहुमत से फैसला
1 अगस्त 2024 को 6-1 के भारी बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को इन कैटेगरीज के भीतर सबसे पिछड़े समुदायों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एससी और एसटी के भीतर सब-कैटेगरी बनाने की अनुमति दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने और जस्टिस मनोज मिश्रा के लिए एक निर्णय लिखा। जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ, पंकज मिथल और एससी शर्मा ने अलग-अलग लेकिन सहमत राय लिखी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी एकमात्र जज असहमत थीं।
क्या सभी अनुसूचित जातियां एक समरूप यूनिट हैं?
इस मामले में एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि क्या अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल सभी जातियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 341(1) राष्ट्रपति को विशिष्ट जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार देता है। ऐसी अधिसूचना के बाद, संविधान यह अनिवार्य करता है कि केवल संसद ही किसी जाति, नस्ल या जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है. दविंदर सिंह के फैसले के माध्यम से, CJI चंद्रचूड़ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि एक निश्चित अनुसूचित जाति सूची में शामिल सभी जातियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।फैसले के पैराग्राफ 112 में उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि सबसे पहले, एससी कैटेगरी में कुछ जातियों को शामिल करना केवल उन्हें अन्य जातियों से अलग करने के लिए है, जो इस श्रेणी में शामिल नहीं हैं और दूसरा, इस तरह के समावेश से स्वचालित रूप से एक समान और आंतरिक रूप से समरूप वर्ग का निर्माण नहीं होता है, जिसे आगे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। वास्तव में सीजेआई ने एससी के बीच विविधता स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक और अनुभवजन्य साक्ष्य पर भरोसा किया, ताकि यह बात स्पष्ट हो सके कि एससी अपने आप में एक समरूप वर्ग नहीं हैं। पैराग्राफ 140 में उन्होंने एक अध्ययन का हवाला दिया जिसमें बताया गया कि कैसे कुछ दलित जातियां अन्य दलित जातियों के खिलाफ अस्पृश्यता का अभ्यास करती थीं और कैसे देश के कुछ हिस्सों में निचली उपजातियों को दलित मंदिरों में प्रवेश से वंचित किया जाता था।सीजेआई विशेष रूप से, अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक मतभेदों के बारे में जागरूक रहे और उन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया. इसी तरह के साक्ष्यों का हवाला देते हुए, प्रभावी रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिन्नैया मामले में सभी अनुसूचित जातियों के साथ समान व्यवहार करने के निष्कर्ष को खारिज कर दिया, बिना उनके सापेक्ष पिछड़ेपन को ध्यान में रखें।
क्या राष्ट्रपति की लिस्ट (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की) पत्थर की लकीर हैं?
इस मामले में एक और महत्वपूर्ण चिंता यह थी कि राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति की सूची (अनुच्छेद 341 के तहत बनाई गई) के भीतर सब-कैटेगरी बनाने में सक्षम हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए, संविधान के दो प्रमुख अनुच्छेदों- अनुच्छेद 15 और 16 पर ध्यान देना आवश्यक है। जबकि अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है। विशेष रूप से अनुच्छेद 15, खंड (4) राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है. इसके अलावा, अनुच्छेद 16, खंड (4) राज्यों को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण प्रदान करने की विशिष्ट शक्ति देता है, जो राज्य की राय में, राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है.दविंदर सिंह केस में बहुमत ने एससी के बीच सब-कैटेगरी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अनुच्छेद 15 और 16 का उपयोग किया. सीजेआई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट रूप से कहा कि अनुच्छेद 15 और 16 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में राज्य सामाजिक पिछड़ेपन की विभिन्न डिग्री की पहचान करने और अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े एससी को विशेष प्रावधान (जैसे आरक्षण) प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है.वास्तव में सीजेआई चंद्रचूड़ ने सब-कैटेगरी करने के लिए राज्य सरकारों की विधायी क्षमता के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए अनुच्छेद 15 और 16 का भी उपयोग किया। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों के उद्देश्य से एससी को सब-कैटेगरी करने की शक्ति अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में दी गई है। जो विधायी क्षमता के बारे में चिंताओं को दूर करती है. गौरतलब है कि अपनी असहमति में न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति की सूची को केवल संसद द्वारा बदला जा सकता है।
जस्टिस गवई ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए स्वीकार किया कि अनुच्छेद 15(4) एक सक्षमकारी प्रावधान है, जो उचित कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त सरकार के विवेक पर छोड़ देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछड़े वर्ग के नागरिकों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है, जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। जस्टिस गवई ने अपनी राय के पैराग्राफ 258 में इसे एक सवाल के रूप में प्रस्तुत किया – अनुच्छेद 15 के तहत अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय, अगर राज्य पाता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर कुछ श्रेणियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और केवल कुछ कैटेगरी के लोग ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित संपूर्ण लाभ का आनंद ले रहे हैं, तो क्या राज्य को ऐसी श्रेणियों के लिए अधिक प्राथमिकता देने से वंचित किया जा सकता है? उनके विचार में, इसका उत्तर नकारात्मक है.उन्होंने कहा कि संविधान के तहत समानता का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि सकारात्मक कार्रवाई का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है और सब-कैटेगरी का उपयोग वास्तविक समानता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है (जो औपचारिक समानता से एक कदम आगे होगा)।
राज्यों को सब-कैटेगरी कैसे करना चाहिए
सब-कैटेगरी को हरी झंडी देते हुए इस बारे में भी सावधानी व्यक्त की कि संरक्षण की आवश्यकता वाली कैटेगरीज को कैसे सब- कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए। सब- कैटेगरी करते समय, राज्यों को अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर यह प्रदर्शित करना होगा कि उप-समूह को व्यापक संरक्षण की आवश्यकता है। राज्यों को सब-ग्रुप को वर्गीकृत करने के लिए उचित तर्क भी प्रदर्शित करना होगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जहां कोई राज्य सरकार सब-कैटेगरी करने का निर्णय लेती है, तो उसके निर्णय की न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सब-कैटेगरी किसी राजनीतिक लाभ के लिए न किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि एससी और एसटी पर क्रीमी लेयर सिद्धांत के लागू होने का मुद्दा विवाद में नहीं था। लेकिन चार न्यायाधीशों ने इस पर विचार किया और टिप्पणी की. न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत को बढ़ा चुका है। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए पहले से लागू क्रीमी लेयर अपवाद को एससी और एसटी के लिए भी लागू करने का प्रस्ताव रखा। जस्टिस विक्रम नाथ, पंकज मिथल और सतीश चंद्र शर्मा ने जस्टिस गवई से सहमति जताई।
आगे क्या होने वाला है
560 से ज़्यादा पन्नों के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण और प्रतिनिधित्व के बारे में कई प्रासंगिक टिप्पणियां कीं। ऐसी सभी टिप्पणियों का जिक्र करने के लिए जगह की कमी है। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 16(4) का उद्देश्य राज्य की सेवाओं में, सभी पदों और ग्रेडों में प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों को न सिर्फ रोजगार मिले, बल्कि उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नत होने का उचित अवसर और संभावना भी मिले। यह टिप्पणी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। बल्कि उन लोगों को वास्तविक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई को लागू करने की ज़रूरत को दर्शाती है, जिन्हें इससे वंचित रखा गया है। जैसा कि उम्मीद थी, फैसले ने काफी तूफान खड़ा कर दिया है। यह देखना बाकी है कि देश भर में राज्य सरकारें इसे कैसे लागू करती हैं।